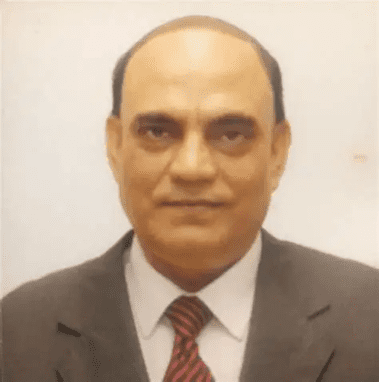- इजराइल का पहला हमला ईरान और अमेरिका के बीच तय छठे राउंड की वार्ता के ठीक एक दिन पहले था। नतीजतन ईरान ने इन वार्ताओं से यह कहते हुए हाथ खींच लिए कि इजरायल की कार्रवाइयों ने बातचीत को असंभव बना दिया है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो हफ्ते के विचार और आकलन के बाद ही किसी निर्णायक कार्रवाई की बात कही थी। पर इस बीच इजरायल का लगातार ईरानी हमले को झेल पाना कठिन होता जा रहा था। तभी अमेरिका को इस क्षेत्रीय युद्ध में अचानक कूदना पड़ा।
- अमेरिका की घरेलू राजनीति में यहूदी समुदाय के विशिष्ट दबदबे के कारण ही अमेरिकी विदेश नीति नियंता कभी भी इजरायली हितों को दरकिनार रखने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते।
- राष्ट्रपति ट्रम्प की विदेश नीति का अमेरिकी हितों की प्राथमिकता पर विशेष जोर तथा अन्य राष्ट्रों के प्रति कठोर एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण, 1945 के बाद के नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से अमेरिका को धीरे-धीरे दूर करता जा रहा है।
- ट्रम्प प्रशासन को दुनिया को यह समझाना मुश्किल होगा कि किस फार्मूले के तहत वह बमबारी करके और युद्धोन्माद बढ़ाकर शांति स्थापित करेंगे।
- भारत के लिए श्रेयस्कर होगा कि वह इजरायल और ईरान को द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर संवाद के जरिए समाधान को बढ़ावा देने की नीति अपनाए।
22 जून को ईरान के तीन प्रमुख परमाणु स्थलों-फोर्डो, नतांज और इस्फहान-पर अमेरिकी बमबारी के बाद इजरायल-ईरान संघर्ष एक खतरनाक एवं विध्वंसात्मक चरण में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका की तरफ से की गई इस कार्रवाई ने; जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता का ‘पूर्ण और सकल विनाश’ बताया है, ने पश्चिम एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है।
हालिया अमेरिकी हमले से पहले, इजराइल और ईरान के बीच जवाबी कार्रवाई की एक श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। इजरायल ने 13 जून को हमले शुरू किए थे। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर ईरान और अमेरिका के बीच तय छठे राउंड की वार्ता के ठीक एक दिन पहले था। ईरान ने बाद में इन वार्ताओं से यह कहते हुए हाथ खींच लिए कि इजरायल की कार्रवाइयों ने बातचीत को असंभव बना दिया है। बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाले राष्ट्रों ओमान और कतर ने भी इजरायल के हमले पर निराशा जाहिर की। ईरान ने तब इजरायल के शुरुआती हमलों का जवाब बैलिस्टिक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन से दिया।
इजरायल को पूरा यकीन था कि शायद उनके अचानक ताबड़तोड़ हमले से, जिसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों, शीर्ष सेनानायकों तथा आणविक संयंत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा, ईरान बुरी तरह डगमगा जाएगा और घुटने टेक देगा। पर आठ दिनों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे ईरान का व्यापक जन मानस पूरी शिद्दत के साथ सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के नेतृत्व में एकजुट हो गया। ईरान ने जब पलटवार करना शुरू किया तो इजराइल के महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों तथा व्यावसायिक स्थलों की काफी नुकसान पहुंचा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह दावा कि हम तेहरान को नेस्तनाबूद का देंगे, युद्ध की धरातलीय हकीकत के समक्ष बेमानी लगने लगा।
ऐसे नाज़ुक मौके पर नेतन्याहू के सामने अमेरिका को युद्ध में शामिल करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। नतीजतन अमेरिका को 21 जून (पश्चिमी एशिया के हिसाब से 22 जून) को युद्ध में कूदने का फैसला लेना पड़ा। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दो दिन पहले ही दो हफ्ते के विचार और आंकलन के बाद ही किसी निर्णायक कार्रवाई की बात कही थी। पर इजरायल के लिए लगातार दो सप्ताह ईरान के जवाबी हमले को झेल पाना कठिन होता जा रहा था। यह एक बड़ा कारण था कि अमेरिका को इस क्षेत्रीय युद्ध में अचानक कूदना पड़ा।
अमेरिकी हस्तक्षेप और फोर्डो नाभिकीय केंद्र
ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को लेकर अमेरिका पहले से ही चिंतित रहा है। इसके विरोध में न केवल बंदिशें लगाईं, वरन विश्व जनमत तैयार करने में भी कोई कोर कसर न उठा रखी। इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं थी कि ईरानी परमाणु क्षमता को ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी सेना ने तीन प्रमुख ईरानी परमाणु संयंत्रों-फोर्डो, नतांज और इस्फहान-पर ‘बड़े पैमाने पर सटीक हमले’ किए हैं।
फोर्डो की नाभिकीय संवर्धन सुविधा; जो एक पहाड़ के नीचे गहराई तक दबी हुई मानी जाती है, को बी-2 स्पिरिट बॉम्बर से गिराए गए जीबीयू-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनिट्रेटर (एमओपी), या ‘बंकर-बस्टर’ बमों से निशाना बनाया गया। जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के परमाणु स्थलों को ‘पूरी तरह से नष्ट’ कर दिया है। खुफिया सूत्रों और हवाई निगरानी की जानकारी रखने वाले अभी भी यह मानते हैं कि ईरान ने पहले ही उच्च संवर्धित यूरेनियम को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया होगा। हमलों से बिजली की आपूर्ति और सेंट्रीफ्यूज कैस्केड को नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन हो सकता है कि सारा संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास सुरक्षित हो। और जहां तक संवर्धन की विधा, ज्ञान और दक्षता का सवाल है उसे समूल नष्ट कर पाना शायद अमेरिका के वश में भी नहीं है।
अमेरिका और इजरायल के संबंध
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यद्यपि किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है, पर यह सिद्धांत अमेरिका और इजरायल के रिश्तों पर लागू नहीं होता। अमेरिका की घरेलू राजनीति में यहूदी समुदाय के विशिष्ट दबदबे के कारण ही अमेरिकी विदेश नीति नियंता कभी भी इजरायली हितों को दरकिनार रखने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद हुए चार अरब-इजराइल युद्धों में अमेरिका की एकतरफा पक्षधरता तथा अभी हाल में इजरायल-हमास संघर्ष में उसकी भूमिका से यह बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है।
राजनयिक चुनौतियां और यूरोप की घटती भूमिका
जब भी हम पश्चिमी एशिया के संघर्षों की बात करते हैं, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं है जो इस क्षेत्र की युद्ध और शांति की शर्तें तय करने की ताकत और हैसियत रखता हो। पूर्व में यह क्षमता कुछ हद तक रूस के पास थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध में उलझे होने के बाद उसकी स्थिति भी एक कारगर खिलाड़ी की नहीं रह गई है।
जहां तक यूरोप का सवाल है, उसमें फ्रांस और जर्मनी सरीखे कुछ मुल्क ईरान के प्रति सहानुभूति जरूर रखते हैं, पर वह नाटो की नीतियों और कार्य प्रणाली; जिस पर निर्णायक अमेरिकी वर्चस्व से इंकार नहीं किया जा सकता, के विरुद्ध खुलकर नहीं जा सकते। अभी हाल के जी-7 राष्ट्रों के कनाडा में हुए महा सम्मेलन के प्रस्तावों में यह बात स्पष्ट रीति से परिलक्षित होती है।
यूरोपीय विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी हमलों से पहले तत्काल युद्धविराम के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ सीधी बातचीत शुरू की थी। हालांकि, अमेरिका द्वारा पहले ही हमले किए जाने के बाद, यूरोप की भूमिका और भी हाशिए पर चली गई है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा है, ‘ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता। वह हमसे बात करना चाहते हैं। यूरोप इसमें मदद नहीं कर पाएगा।’
स्पष्ट रूप से यूरोपीय ‘सहयोगियों’ को पूर्व चेतावनी दिए बिना एकतरफा अमेरिकी कार्रवाई, यूरोप के सीमित प्रभाव को पुष्ट करती है, जिससे वे हमलों की निंदा करने और रणनीतिक प्रयासों का नेतृत्व करने के बजाय तनाव कम करने का आह्वान करते हैं।
ट्रंप की विदेश नीति और ‘अमेरिका फर्स्ट’
ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का ट्रंप का निर्णय उनकी ‘अमेरिका फर्स्ट’ विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव या शायद एक पुनर्व्याख्या को दर्शाता है। हालांकि, उन्होंने विदेशी उलझनों से अमेरिका को बाहर निकालने का अभियान चलाया था, लेकिन यह कार्रवाई सीधे तौर पर अमेरिका को एक पेचीदे संघर्ष में घसीटे जाने की शुरुआत है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की विदेश नीति का अमेरिकी हितों की प्राथमिकता पर विशेष जोर तथा अन्य राष्ट्रों के प्रति कठोर एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण, 1945 के बाद के नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से अमेरिका को धीरे-धीरे दूर करता जा रहा है। इस नीति की मुख्य विशेषता रही है कि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) के सिद्धांत का पालन करते हुए अमेरिका घरेलू हितों से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देगा। पर यहां एक अंतर्विरोध है कि ‘अमेरिका फर्स्ट’ की विदेश नीति ट्रम्प प्रशासन के कड़े इजरायल-समर्थक रुख के साथ मेल नहीं खाती।
क्या अब भी मिलेगा ट्रम्प को शांतिदूत का खिताब?
क्या यह हमले ट्रंप को ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने का प्रयास करने के लिए ‘शांतिदूत’ का खिताब दिला सकेंगे, बावजूद इसके कि इसका तात्कालिक परिणाम संघर्ष में खतरनाक वृद्धि की ओर इंगित करता है? कोई कुछ भी कहे, ट्रम्प प्रशासन को दुनिया को यह समझाना मुश्किल होगा कि किस फॉर्मूले के तहत वह बमबारी करके और युद्धोन्माद बढ़ाकर शांति स्थापित करेंगे। साथ में राष्ट्रपति ट्रम्प को शांति के मसीहा के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होंगे। हां, अमेरिका के पास अब एक आखिरी मौका है कि इस हमले के बाद वह इजरायल को युद्ध विराम के लिए राजी कर ले। पर क्या ऐसे प्रस्ताव को नेतन्याहू और उनकी सरकार स्वीकार करेगी?
ईरान की परमाणु स्थिति और अंतरराष्ट्रीय निगरानी
ईरान ने लगातार दावा किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को इसके विपरीत सबूत मिले हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) ने इजरायल के शुरुआती हमलों से कुछ घंटे पहले ईरान को अपनी निगरानी प्रयासों के साथ गैर-अनुपालन की श्रेणी में घोषित किया और ईरान के जटिल और बढ़ते परमाणु कार्यक्रम की निगरानी रख पाने की अपनी क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह व्यक्त किया था।
फोर्डो में 84 फीसदी शुद्धता (हथियारों-ग्रेड के करीब) तक संवर्धित यूरेनियम कण 2023 की शुरुआत में पाए गए थे, और ईरान ने नतांज और फोर्डो में बढ़ी हुई गति से संचालन फिर से शुरू कर दिया था, जिसमें यूरेनियम को 60 फीसदी तक संवर्धित किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के के कदम को ‘साहसिक निर्णय’ कहकर सराहना करते हुए अमेरिकी कार्रवाइयों के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वह ‘इतिहास बदल देंगे।’ दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री ने हमलों को ‘क्रूर’ बताया, ‘स्थायी परिणामों’ की चेतावनी दी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह किया, ताकि अमेरिका की निंदा की जा सके। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने भी हमलों की अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए निंदा की और अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ‘खतरनाक वृद्धि’ और संघर्ष के नियंत्रण से बाहर होने के ‘बढ़ते जोखिम’ पर ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त की, इस बात पर जोर देते हुए कि मौजूदा संकट का ‘कोई सैन्य समाधान नहीं’ हो सकता। उन्होंने सभी पक्षों से तनाव कम करने और कूटनीति पर लौटने का आग्रह किया।
चीन और रूस का रुख
चीन और रूस दोनों ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हमलों की ‘कड़ी निंदा’ की है, उन्हें ‘अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन’ बताया है। रूस ने भी चेतावनी दी है कि वाशिंगटन की वैश्विक विश्वसनीयता को झटका लगा है।
चीन इस हमले को ‘अमेरिका के लिए एक रणनीतिक गतिरोध’ के रूप में देखता है और युद्ध विराम और राजनयिक समाधान के प्रयासों को प्राथमिकता देने की पेशकश करता रहा है। चीन पश्चिमी एशिया में गैर-हस्तक्षेप को नैतिक मानदंड को आधार बनाए रखने और क्षेत्र के आर्थिक भविष्य के साथ संतुलित करने का समर्थक है।
चीन की फौरी प्रतिक्रियाएं, हालांकि आलोचनात्मक हैं, अमेरिका के साथ सीधे सैन्य टकराव में शामिल होने की अनिच्छा को दर्शाती हैं, जो निश्चित रीति से पश्चिम एशिया में अमेरिकी शक्ति के स्थायी प्रभुत्व को उजागर करती हैं।
क्षेत्रीय दृष्टिकोण और भारत की भूमिका
ईरान ने अमेरिकी हमलों का बदला लेने की कसम खाई है, और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को धमकी दी है। दुनिया ईरान की भावी प्रतिक्रिया और कार्रवाई का इंतजार कर रही है।
यद्यपि अनेक इस्लामी मुल्कों ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है, जिसमें ‘मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा’ और क्षेत्रीय स्थिरता के जोखिमों की चेतावनी दी गई है, पर कहीं से भी ईरान के लिए आर्थिक या सैन्य मदद की बात अभी तक सामने नहीं आए है। इसलिए इस हमले का तात्कालिक परिणाम युद्ध की विभीषिका में खतरनाक वृद्धि और इजराइल-ईरान संघर्ष के नियंत्रण से बाहर होने का जोखिम ही बढ़ाएगा!
भारत के लिए इजरायल-ईरान युद्ध और अमेरिका द्वारा ईरान के आणविक संयंत्रों पर सीधे बमबारी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया दे पाना कठिन है। इतना ही कहा जा सकता है कि चूंकि भारत युद्ध के विरोध में रहा है और एक ऐसा युद्ध; जिसमें वे दो राष्ट्र शामिल हों जिनसे हमारे राजनयिक एवं व्यावसायिक संबंध हों, हमें संतुलन बनाकर चलना होगा। इजरायल और ईरान को द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर संवाद के जरिए समाधान को बढ़ावा देने की नीति अपनाना ही श्रेयस्कर होगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चुनौती
यह कहना अनुचित न होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष एक बड़ी चुनौती है; एक लंबी टकराव के जोखिमों को बातचीत के माध्यम से हल करना तथा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना।
वर्तमान संकट इस बात को स्पष्ट रीति से रेखांकित करता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में रणनीतिक परिदृश्य को निर्णायक रूप से बदलने में सक्षम एकमात्र नगरी शक्ति है, और क्षेत्र में शांति और स्थिरता वाशिंगटन में लिए गए एकतरफा फैसलों पर निर्भर करती है। सत्यापित परमाणु रियायतों तथा बातचीत के माध्यम से युद्ध विराम की पहल, जिस कुशल कूटनीति की मांग करता है, वह हाल की कार्रवाइयों में सिरे से नदारद है।
एक सकारात्मक बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद लक्षित ईरानी परमाणु स्थलों पर बाहरी विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। हालांकि, ईरान की परमाणु सुविधाओं को हुए नुकसान की पूरी सीमा की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्ण विनाश के दावों के बावजूद, खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हमलों से पहले अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को स्थानांतरित कर दिया होगा और यद्यपि हमलों ने बिजली की आपूर्ति और सेंट्रीफ्यूज कैस्केड को नुकसान पहुंचाया होगा, उन्होंने शायद सभी संवर्धित यूरेनियम या परमाणु प्रौद्योगिकी में ईरान द्वारा अर्जित ज्ञान और दक्षता को नष्ट नहीं किया है।
पश्चिमी एशिया जैसे एक अत्यधिक अस्थिर क्षेत्र में व्यापक संघर्ष को रोकने तथा तनाव कम करने के लिए बड़े पैमाने पर राजनयिक समाधान की तत्काल आवश्यकता है। मौजूदा परिस्थितियों में यह कैसे संभव होगा, इसका उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है।